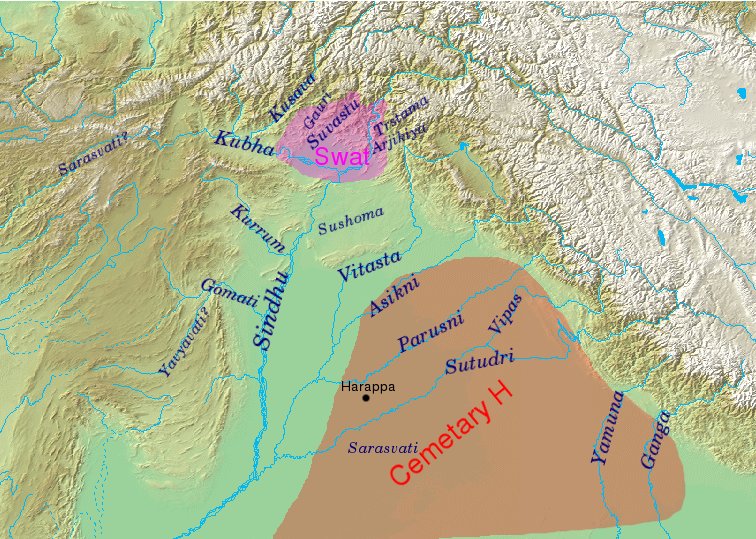इस वाकये को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जगह थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अमरनाथ झा हॉस्टल, जो कभी म्योर हॉस्टल हुआ करता था जिसे अंग्रेज़ीदां लोग अब भी म्योर हॉस्टल ही कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। मौका था हॉस्टल के सोशल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव। चार-पांच सीनियर्स और बाकी नए बैच के हम जैसे पंद्रह-बीस छात्रों ने ठान लिया कि इस बार हम हिदी के मसले को लेकर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे।
इस वाकये को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जगह थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अमरनाथ झा हॉस्टल, जो कभी म्योर हॉस्टल हुआ करता था जिसे अंग्रेज़ीदां लोग अब भी म्योर हॉस्टल ही कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। मौका था हॉस्टल के सोशल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव। चार-पांच सीनियर्स और बाकी नए बैच के हम जैसे पंद्रह-बीस छात्रों ने ठान लिया कि इस बार हम हिदी के मसले को लेकर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे।असल में हम हॉस्टल में रहने लगे तो पता चला कि सभी छात्रों को एसी और डीसी समुदायों में बांटने सिलसिला वहां की परंपरा में है, जिसमें ए से अंग्रेजी और डी से देहाती हुआ करता था। सी का मतलब आप खुद समझ लीजिए, सभ्यता के तकाजे के चलते उसे मैं लिख नहीं सकता। कॉन्वेंट में पढ़े अफसरों या अमीर घरों से आए छात्र एसी कहलाते थे, जबकि हिंदी माध्यम से पढ़कर आए छात्र डीसी कहलाते थे। हमें यह नामकरण बड़ा अपमानजनक लगता था। इसीलिए हमने ठान ली कि इस बार हॉस्टल में सभी डीसी लोगों को एकजुट अपने ही बीच का सोशल सेक्रेटरी बनाएंगे।
सोशल सेक्रेटरी की खास अहमियत थी क्योंकि वही हर साल होनेवाले फेस्टिवल उदीसा में हॉस्टल का प्रतिनिधित्व करता था। हमने हिंदी के मसले पर चुनाव लड़ा और संख्या के बल पर चुनाव जीत भी गए। हालांकि चुनाव के ठीक पहले की रात दोनों ही पक्षों ने छात्रों को तोड़ने के लिए खूब जोड़तोड़ की। भेदिए लगाए गए। मुझ जैसे डीसी को एक सीनियर ने मॉडल्स की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि तुम इनमें से किसको पसंद करते हो। मैंने जब अपनी पसंद बता दी तो सीनियर ने कहा कि पसंद बताती है कि तुम डीसी नहीं हो। हमारी तरफ से मेधावी छात्रों ने बडी-बड़ी बातें करके एसी कैंप में फूट डाली और कामयाब भी रहे।
आखिरकार नतीजा आया तो डीसी प्रत्याशी भारी मतों के अंतर के साथ जीत गया। तय हुआ कि कुछ ही बाद होनेवाले उदीसा फेस्टिवल में वह अपना भाषण हिंदी में देगा। देश को गुलामी से लेकर आज़ादी के बाद तक देश को सबसे ज्यादा आईएएस देनेवाले म्योर हॉस्टल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। एसी लॉबी में खलबली मच गई। एक्स-म्योरियंस को बुलाया गया। उन्होंने अंग्रेजियत का ऐसा दबाव बनाया कि हिंदी के नाम पर जीते सोशल सेक्रेटरी के लिए जब उदीसा में बोलने की बारी आई तो उसने अंग्रेजी में भाषण दे डाला। हम सभी के लिए यह भारी पराजय थी। हॉस्टल के अधिकांश छात्रों ने उस पूरे समारोह का बहिष्कार कर दिया।
 आज हिंदी दिवस के मौके पर उस वाकये की याद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तलवारें खींचकर या लामबंदी करके न तो अंग्रेजी को हटाना संभव है और न ही हिंदी को स्थापित करना। भाषा लंबे समय में स्थापित होती है और इसका निर्धारण जीवन स्थितियां ही करती हैं। सत्ता का जिस तरह से हस्तांतरण हमारे यहां हुआ है, उसे देखते हुए अनुवाद या सरकारी कोशिशों से हिंदी को हिंदुस्तान में जन-जन की भाषा नहीं बनाया जा सकता।
आज हिंदी दिवस के मौके पर उस वाकये की याद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तलवारें खींचकर या लामबंदी करके न तो अंग्रेजी को हटाना संभव है और न ही हिंदी को स्थापित करना। भाषा लंबे समय में स्थापित होती है और इसका निर्धारण जीवन स्थितियां ही करती हैं। सत्ता का जिस तरह से हस्तांतरण हमारे यहां हुआ है, उसे देखते हुए अनुवाद या सरकारी कोशिशों से हिंदी को हिंदुस्तान में जन-जन की भाषा नहीं बनाया जा सकता।हां, हिंदी फिल्मों ने, टीवी सीरियलों ने और अब हिंदी टीवी न्यूज ने पूरे देश में हिंदी को ज्यादा ग्राह्य बना दिया है। हम भले ही बाज़ार को गाली दे लें, लेकिन बाज़ार भी हिंदी के मानकीकरण और विस्तार में मदद कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल के प्लेटफॉर्म पर हिंदी का आना, यूनिकोड फॉन्ट का आना, हिंदी के ब्लॉगों की बढ़ती संख्या, विज्ञापनों में हिंदी और हिंग्लिश का बढ़ता चलन इस बात को स्थापित करने के लिए काफी हैं।
कुछ दिन पहले ही आईबीएम के सीईओ सैमुअल पामिसैनो ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था, जिसमें इंडिया ऑनलाइन सर्वे के हवाले से बताया था कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करनेवालों के बीच अंग्रेजी की धाक बहुत तेज़ी से गिर रही है। साल भर पहले जहां 59 फीसदी लोग अंग्रेजी में ब्राउज करते थे, वहीं अब इनका अनुपात 41 फीसदी रह गया है। शायद भोमियो या अनुवाद का स्कोप तेज़ी से बढ़ रहा है।
हिंदी के साथ एक और समस्या है, जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं। हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं – ब्रज से लेकर अवधी और भोजपुरी तक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के साथ बोलियां मिट रही हैं। आज शहर में नौकरी कर रहा कोई परिवार अवधी में बात करना पसंद नहीं करता। ये अलग बात है कि भोजपुर भाषियों के साथ ऐसा नहीं है। मैं भाषाविद नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बोलियों और उत्तर भारत की भाषाओं के साथ एकीकरण के बिना हिंदी को स्वीकार्य और व्यापक नहीं बनाया जा सकता।
अंत में भाषा के राष्ट्रीय आग्रह के बारे में एक छोटा-सा अनुभव सुनाना चाहता हूं। जर्मनी से लौटने के दौरान सभी मित्र एक-दूसरे से अपने पतों का आदान-प्रदान कर रहे थे। इसी में चीन का भी एक मित्र था। मैंने सभी को अपना भारतीय पता अंग्रेजी में लिखकर दिया था। भारत पहुंचकर मैं एक दिन अपनी डायरी देख रहा था तो मैंने पाया कि चीन के उस मित्र ने तो अपना पता चीनी भाषा में लिखा है, बस फोन नंबर और पिन कोड ही अंग्रेजी में हैं।